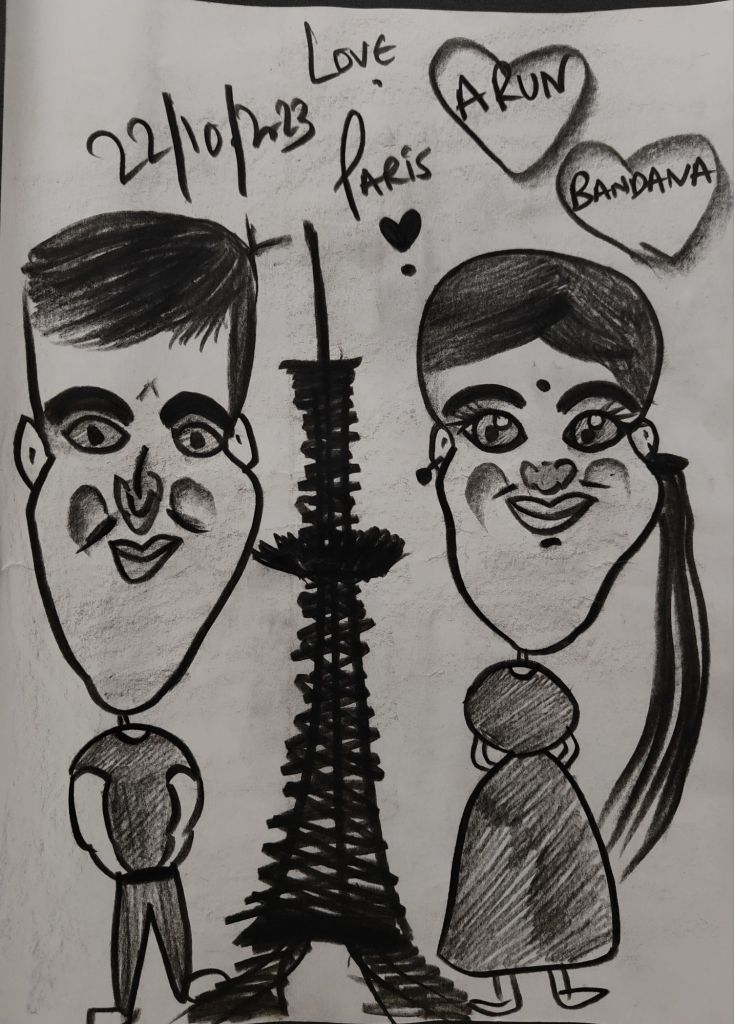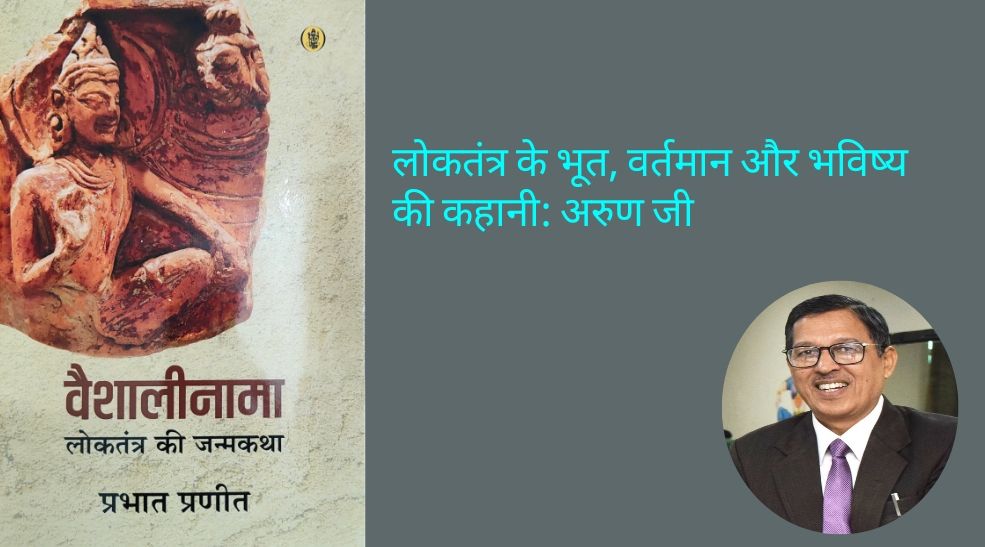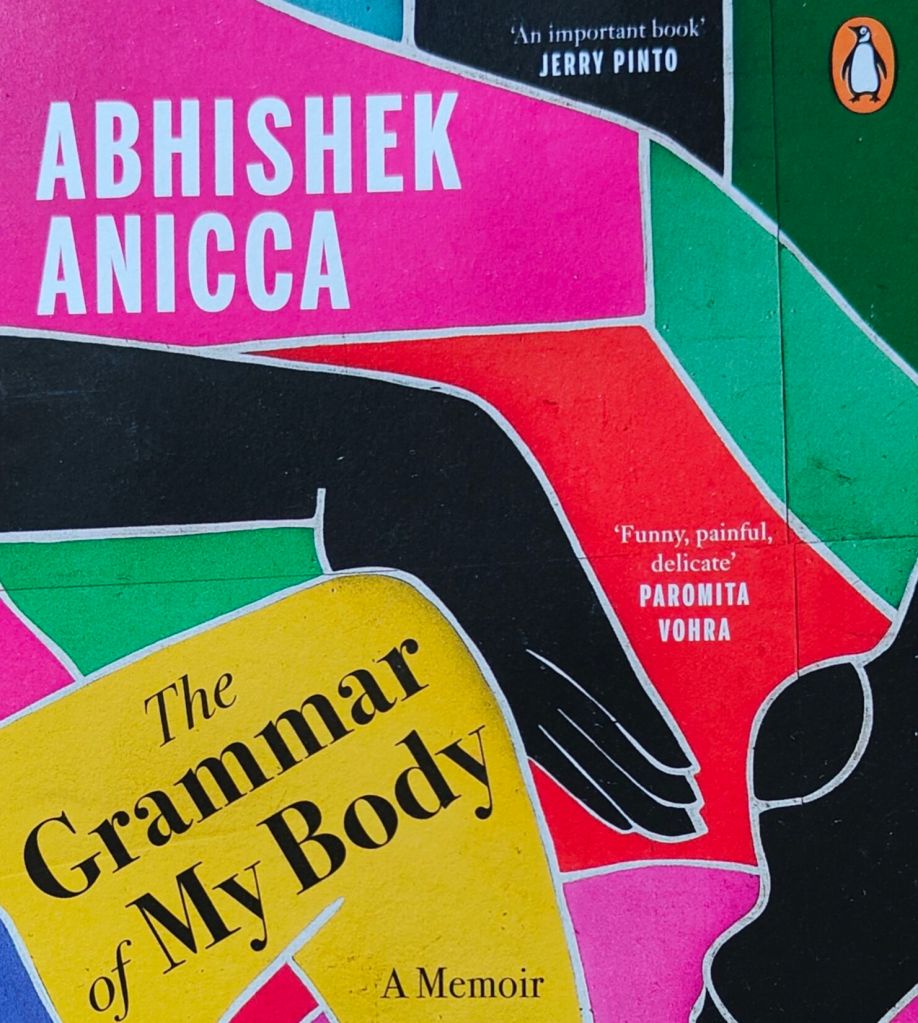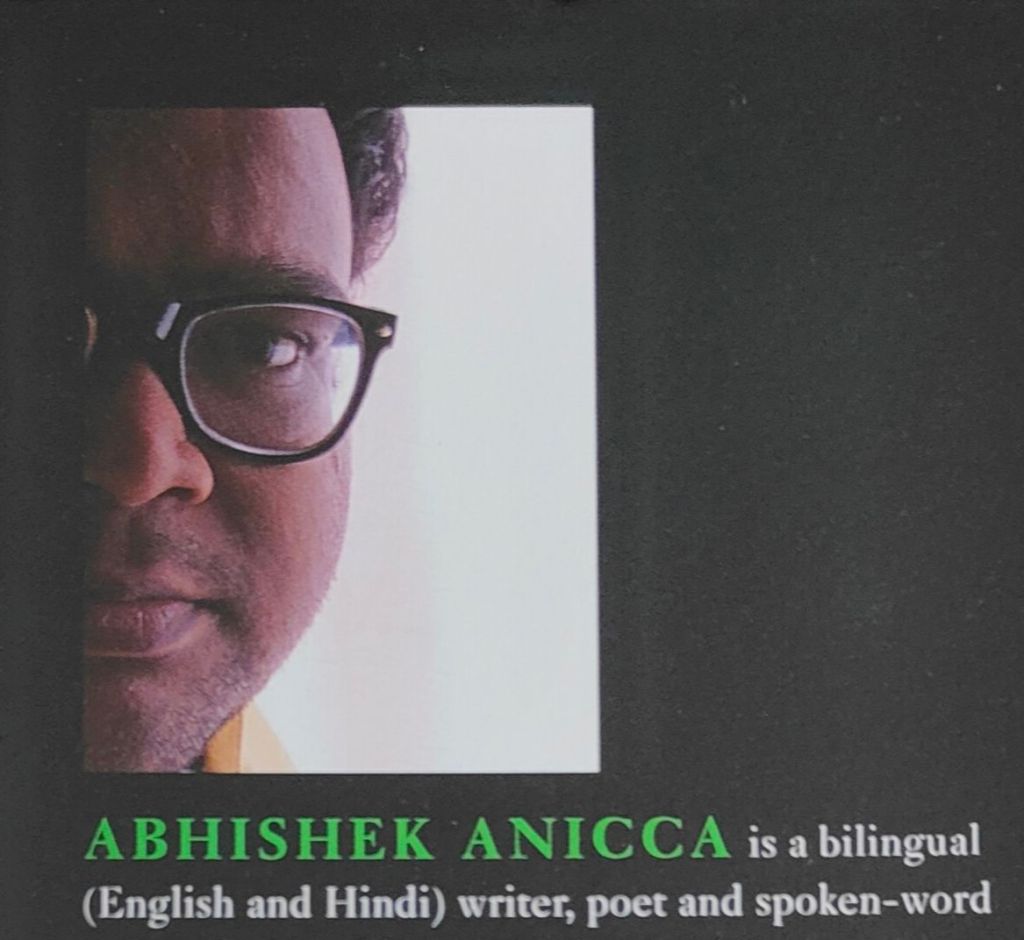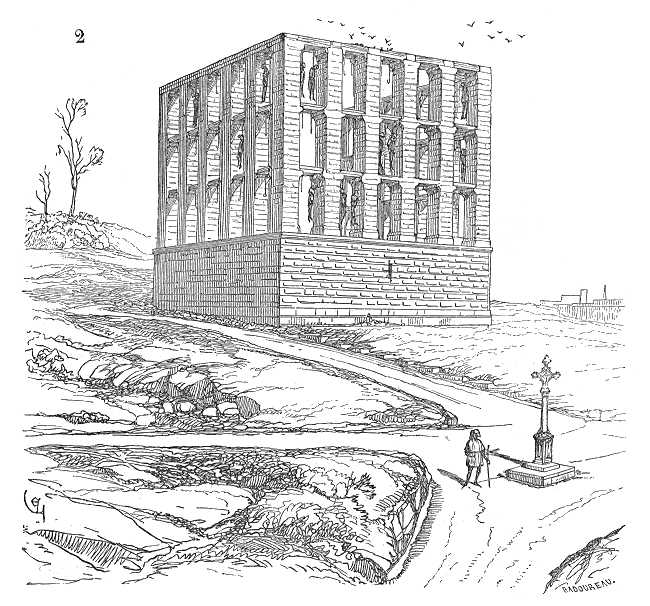पिछले महीने मशहूर अनुवादक डेज़ी रॉकवेल ने X (ट्विटर) पर घोषणा की: अब मैं X को छोड़ रही हूं। मुझसे जुड़ने के लिए आप Blue Sky पर आ सकते हैं। मेरे कान खड़े हो गए। मन में कई सवाल उठने लगे। कि अचानक ये क्या हुआ कि डेज़ी रॉकवेल जैसी अंतर्राष्ट्रीय ख़्याति प्राप्त अनुवादक X छोड़ रही हैं? और ये ब्लू स्काय कौन सी बला है जिसे वह और उनके जैसे अन्य कई लेखक, अनुवादक, कवि, मीडिया संस्थान ज्वाइन कर रहे हैं?
ढूंढ़ने पर पता चला कि ब्लू स्काय एक माइक्रोब्लॉगिंग साइट है। इसका होम पेज असंख्य तारों से भरे नीले आसमान की तरह दिखता है। ठीक अपने नाम के अनुरूप। स्वच्छ एवं पारदर्शी। 2019 में इसे ट्विटर ने ही शुरू किया था। एक प्रयोग के तौर पर। उस वक्त यह आम लोगों के लिए उपलब्ध नहीं था। 2022 में ट्विटर पर एलोन मस्क के स्वामित्व के बाद ब्लू स्काय से ट्विटर का रिश्ता टूट गया। इसका अपना एक स्वतंत्र वजूद हो गया। हालांकि आम लोगों के लिए इसका दरवाज़ा खुला इस वर्ष, फ़रवरी 2024 में।
पर अचानक इतनी बड़ी संख्या में X को छोड़ लोग ब्लू स्काय की ओर क्यों भागने लगे? और ख़ासकर पिछले दो महीनों में भागने की इस क्रिया में अप्रत्याशित वृद्धि कैसे हुई? इन प्रश्नों के उत्तर मुझे मिलने लगे X और उसके स्वामी एलोन मस्क की हाल की गतिविधियों पर नज़र डालने पर।
2022 में जब से मस्क ने ट्विटर की कमान संभाली, उसका नाम बदल कर X रखा, तभी से उसपर बदलाव दिखने लगे थे। खरीदने के पहले मस्क ने काफी प्रचार किया था कि वे स्वतन्त्र विचारों (Free Speech) को बढ़ावा देंगे, गलत सूचनाओं पर नियंत्रण करेंगे वगैरह वगैरह। पर किया उन्होंने ठीक उसका उल्टा।
आते ही उन्होंने उन कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जो ट्विटर पर घृणा या झूठ को रोकने में लगे थे। उसके बाद उन्होंने 62000 ऐसे निलंबित एकाउंट्स को बहाल किया जिनका प्रयोग झूठ और घृणा फैलाने के लिए किया जा रहा था। फिर डोनाल्ड ट्रम्प के एकाउंट को बहाल किया। वही एकाउंट जिस पर कैपिटोल हिल पर हमले के लिए उकसाने का आरोप था।
ट्विटर का नया अवतार X धीरे धीरे एक पार्टी, एक विचारधारा के पक्ष में दिखने लगा। मस्क खुद भी वहां रिपब्लिकन पार्टी का प्रचार करने लगे। ट्रम्प के पक्ष में और कमला हैरिस के विरोध में झूठ फैलाने लगे। ग़लत तथ्यों, झूठे विडियो का प्रयोग करने लगे। वैसे किसी पार्टी, व्यक्ति या विचार के पक्ष में होना ग़लत नहीं है। पर वह जिस तरीके से कर रहे थे, उससे उनकी निष्पक्षता और उससे भी ज्यादा X की निष्पक्षता पर सवाल उठने लगे।
मस्क साहब केवल वहीं नहीं रुके। द वाशिंगटन पोस्ट में माईकल शीरर एवं जोश डोअसी की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी चुनाव में डोनाल्ड ट्रम्प को जिताने में लगी 45 मिलियन डॉलर के एक प्रोजेक्ट का नेतृत्व करने लगे। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसकी बहुत सारी चीज़ें अस्पष्ट थीं। जैसे किन लोगों ने उसमें डोनेशन दिया, कितना दिया वगैरह वगैरह। प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य था कमला हैरिस के समर्थकों को झांसा देकर ट्रम्प के पक्ष में रिझाना। और उन्हें बहकाना।
इस काम के लिए उनके पास सलाहकारों की एक पूरी फौज थी। अत्यंत आधुनिक तकनीकों से लैस। वे अमरीकी वोटरों के विचार, उनके व्यक्तिगत पसंद, नापसंद से अवगत थे। उन्होंने इस पर अच्छा-खासा रिसर्च किया था। उन्हें मालूम था कि अमरीका के किस स्टेट, किस क्षेत्र के वोटर को किस तरह का मेसेज, विडियो या ऑडियो भेजना है। और कैसे भेजना है।
यहूदी वोटरों को मेसेज भेजा गया कि कमला हैरिस इज़राइल-फिलीस्तीन मुद्दे पर फिलीस्तीनियों की समर्थक हैं। मुसलमान वोटरों को मेसेज भेजे गए कि कमला के पति यहूदी है और वह इज़राइल की समर्थक हैं। उदारवादियों को बताया गया कि कमला रूढ़िवादी हैं और रूढ़िवादियों को कि वे उदारवादी हैं। अश्वेत वोटरों को कहा गया कि कमला के आने से उनके अधिकारों का हनन होगा। श्वेतों को डराया गया कि अश्वेत को ज्यादा लाभ दिये जाएंगे।
ई-मेल, सोशल मीडिया में टेक्स्ट, ओडियो, विडियो के माध्यम से खूब प्रचार किया गया। झूठ, आधा सच का धड़ल्ले से प्रयोग हुआ। वोटरों की शिनाख़्त करके, सटीक निशाना बनाकर उन्हें इस तरह कन्फ्यूज़ किया गया कि वे कमला हैरिस से विमुख हो जाएं। चुनाव से एक सप्ताह पहले इस प्रचार तंत्र ने अपनी गतिविधियां और तेज कर दीं। इसका वोटरों पर अपेक्षित असर हुआ। डोनाल्ड ट्रम्प जीत गए।
जीत के बाद जब डोनाल्ड ट्रम्प ने ऐलान किया कि अमरीका में ‘एलोन मस्क नामक एक नये सितारे का उदय हुआ है’ तब लोगों को आश्चर्य नहीं हुआ। क्योंकि वैसे भी X पर मस्क की गतिविधियां जगजाहिर थीं। रही-सही का पर्दाफाश द वाशिंगटन पोस्ट, अल्जज़ीरा जैसे मीडिया संस्थानों ने कर दिया।
यही वो समय था जब ब्लू स्काय का उदय हुआ। सोशल मीडिया के एक नये सितारे के रूप में। फ़रवरी 2024 में जैसे ही ब्लू स्काय की खिड़की खुली, लोग X को छोड़ उससे जुड़ने लगे। वे X के पक्षपातपूर्ण रवैए से उब चुके थे। ख़फ़ा थे। अमरीकी चुनाव के नजदीक आने के साथ-साथ ब्लू स्काय पर भीड़ बढ़ने लगी। पिछले दो महीनों में (अक्टूबर 2024 से) ट्विटर से भागकर ब्लू स्काय ज्वाइन करने वालों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि होने लगी।
द गार्डियन के अनुसार पिछले दो महीनों में क़रीब 2.7 मिलियन अमरीकी यूज़र्स मस्क के X को छोड़ चुके हैं। और उसी अवधि में ब्लू स्काय में क़रीब 2.5 यूज़र्स की वृद्धि हुई। जैसे जैसे अमेरिका में चुनाव के दिन नजदीक आने लगे, वैसे वैसे इसमें तेजी आने लगी। ट्रम्प की जीत के बाद इसमें और भी तेजी आई। 5 नवंबर को चुनाव परिणाम घोषित हुए और उसके एक सप्ताह के अंदर ब्लू स्काय के यूज़र्स की संख्या 743900 से बढ़कर 1400000 (1.4 मिलियन) हो गई। मतलब दूनी हो गई। उसके अगले सप्ताह में एक बार फिर से दूनी हुई, मतलब 2.8 मिलियन।
X को छोड़ ब्लू स्काय ज्वाइन करने वालों में दुनियां भर के जाने-माने फिल्मकार, कलाकार, साहित्यकार, पत्रकार, मीडिया संस्थान, सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। 26 नवंबर को यूरोपीय फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट्स ने घोषणा की कि 20 जनवरी 2025 से वे एलन मस्क के X पर कुछ भी प्रकाशित नहीं करेंगे। वे X का हिस्सा इसलिए नहीं बनना चाहते क्योंकि एलोन मस्क ने उसे झूठ और प्रोपगंडा फैलाने की मशीन के रूप में परिवर्तित कर दिया है। यूरोपीय फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट्स एक ऐसी संस्था है जिससे 44 देशों के 295000 जर्नलिस्ट्स जुड़े हैं। 13 नवंबर को इंग्लैंड के जाने-माने न्यूज़ पोर्टल द गार्डियन ने घोषणा की: X पर वह अपने आधिकारिक हैंडल से कुछ भी पोस्ट नहीं करेगा। अन्य देशों के मीडिया संस्थान एवं नामी हस्तियां भी धीरे-धीरे X को छोड़ रहे हैं। ब्लू स्काय में यूज़र्स की संख्या रोज-ब-रोज तेजी से बढ़ रही है।
सोशल मीडिया के फ़लक पर 3000 मिलियन यूज़र्स के साथ मार्क जुकरबर्ग का फ़ेसबुक आज भी सबसे आगे है। 2500 मिलियन के साथ गूगल का यूट्यूब दूसरे नंबर पर है। इसके बाद मार्क जुकरबर्ग के ही इन्स्टाग्राम में 2350 मिलियन यूज़र्स, व्हाट्सएप में 2400 मिलियन और मेसेंजर में 1000 मिलियन यूज़र्स हैं। हरेक की अपनी अपनी खासियत है। पर ब्लू स्काय की तुलना इनमें से किसी से नहीं हो सकती। वह X एवं Threads की तरह एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है जिसका उद्देश्य है कम-से-कम शब्दों में सूचना व समाचार को तत्काल शेयर करना।
ब्लू स्काय के यूज़र्स की संख्या अभी 20 मिलियन से कुछ अधिक है। ये X के 500 मिलियन और Threads के 275 मिलियन से अभी भी काफ़ी कम है। पर जिस तेजी से लोग इसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि आने वाले महीनों एवं वर्षों में यह इन दोनों के लिए खतरे की एक बड़ी घंटी है।
ब्लू स्काय एक मायने में इन दोनों से बिल्कुल भिन्न है। यह एक ओपन सोर्स प्लेटफार्म है जो मुनाफे के लिए नहीं बना है। कम-से-कम अभी तक तो नहीं। यह लोगों के डोनेशन पर निर्भर है। जब कि X एवं Threads दोनों अमरीका के दो बड़े पूंजिपतियों के हाथों की कठपुतली हैं। हम सब जानते हैं कि X को मस्क कैसे एक औजार की तरह उपयोग कर रहे हैं। मेटा के मालिक मार्क जुकरबर्ग का दामन भी कोई साफ़ नहीं है। उनसे भी लोगों को आशा नहीं है कि Threads का प्रयोग वह निष्पक्ष होकर करेंगे।
ब्लू स्काय की लोकप्रियता का एक और कारण यह है कि यह यूज़र्स को अपने पसंद के लोगों, उनके विचारों से जुड़ने की कुछ खास सुविधाएं प्रदान करता है। साथ ही ये झूठ, प्रोपगंडा और घृणा से दूरी बनाने में मदद करता है। आप चाहें तो यहां अपने मनमुताबिक एक ईको चेम्बर का निर्माण कर सकते हैं। अपने पसंद की चीजें पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं।
हालांकि अपने ईको चेम्बर में रहने और अपने मन की बात सुनने के कुछ नुकसान भी हैं। दूसरे पक्ष से बातचीत व संवाद से वंचित होने का खतरा बना रहता है। फिर भी ब्लू स्काय का वह चेम्बर एक पूंजीपति द्वारा संचालित उस चेम्बर से तो लाख गुना बेहतर है जहां आप बार-बार ठगे से महसूस करते हैं।
———————————–
अरुण जी, 16.12.24